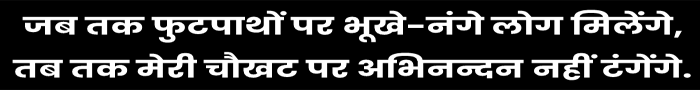देहरादून। होलिका दहन पर जहां देशभर के अधिकतर इलाकों में होलिका जलाई जाती है, वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में चीर बंधन की परंपरा है। ऐसा नहीं है कि यहां होलिका दहन नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में चीर बंधन होता है। इसे भी होलिका का ही प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन को होली के अहम हिस्से के तौर पर देखा जाता है। इस दिन होलिका की पूजा के बाद परिवार के साथ होलिका दहन किया जाता है, लेकिन उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में होलिका दहन से ज्यादा चीर बंधन का महत्व देखने को मिलता है।
हालांकि कई जगहों पर होलिका दहन भी किया जाता है, लेकिन यहां चीर बंधन की परंपरा अधिक रही है। चीर बंधन का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, जिसमें पद्म (पयों) की डाल पर चीर यानी रंग-बिरंगे कपड़े बांधे जाते हैं। इस प्रकार चीर बंधन के साथ कुमाऊं में होली की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि बदलते समय के साथ अब पयों की जगह बांस ने भी ले ली है। इस पर चीर बांधा जाता है। साथ ही परंपरा का निर्वाह करते हुए पयों की एक शाखा इसमें बांध दी जाती है।
कुमाऊं में चीर बंधन लंबे समय से किया जा रहा है। यहां लोग चीर को होलिका का ही प्रतीक मानते हुए पूजन करते हैं। रंग एकादशी के दिन गांव में आंवले के पेड़ के पास एक दंड यानी डंडे में चीर बांधा जाता है। गांव के हर घर से चीर यानी कपड़ा आता है। इन रंग-बिरंगे कपड़ों को दंड में बांधकर इसकी पूजा की जाती है और गांव के एक व्यक्ति को इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। एकादशी के दिन से होली के दिन यानी छरड़ी तक घर-घर में खड़ी होली गाई जाती है। इस दौरान चीर की जिम्मेदारी संभालने वाला शख्स इसे पकड़े हुए सबसे आगे रहता है और हर घर में चीर को गुलाल लगाया जाता है।
होली वाले दिन पूजन के बाद चीर को गांव के लोगों में बांट दिया जाता है। इसे घर के दरवाजे पर लगाया जाता है। माना जाता है कि इससे घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और रोग-दोष, कष्ट आदि का निवारण होता है। हालांकि कुमाऊं में कई जगहों पर होलिका दहन के दिन चीर को पूरे गांव में घूमने के बाद जलाने की परंपरा भी है। इसके अलावा चीर को गांव के मंदिर या सार्वजनिक स्थानों पर भी बांधा जाता है।
उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार चारु तिवारी ‘चीर बंधन’ की परंपरा को लेकर बताते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई यह कहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि कुमाऊं के गांवों में होली का त्योहार काफी बाद में आया। यह शहरों में होलिका दहन के रूप में मनाया जाता था, लेकिन पहाड़ों में त्योहार ऋतुओं से संबंधित थे। यहां ऋतुरैण (चैत्र के महीने में गाया जाने वाला लोकगीत) गाया जाता था और लोक पर्व फूलदेई आदि का ज्यादा महत्व था। चूंकि 15वीं शताब्दी में कुमाऊं के चंद राजाओं के दरबार में होली मनाने की परंपरा शुरू हुई इसलिए माना जाता है कि चीर बंधन की शुरुआत का कालखंड भी अधिक पुराना नहीं है।
वह बताते हैं कि पुराने समय में सामंतों की ओर से चुने गए गांवों को ही चीर दी जाती थी। चीर एक तरह से राजाओं के सांस्कृतिक प्रतीक हो सकते हैं, जो उन्होंने अपने प्रशंसकों को दिए। इसलिए हर गांव में चीर बंधन की परंपरा नहीं थी। बाद में समय के साथ इसका विस्तार हुआ। कालांतर में चीर हरण की परंपरा शुरू हुई। इसमें जिस गांव में चीर बंधन नहीं होता था, वहां के लोग दूसरे गांव की चीर लूटकर लाते थे और अगली होली पर उस गांव में चीर बंधन होता था। वहीं जिस गांव की चीर लूट ली जाती थी, वहां तब तक होली नहीं मनाई जाती थी जब तक वह किसी और गांव से चीर नहीं लूट लाता। इसलिए चीर की सुरक्षा गांव के बलवान युवक करते थे। वर्तमान में चीर हरण की परंपरा न के बराबर दिखती है और अब भाईचारे और सौहार्द के साथ चीर बंधन और होली मनाई जाती है।
वह कहते हैं कि चीर बंधन में चीर को पयों की डालियों की लकड़ी में बांधने का अर्थ प्रकृति से मनुष्य के अंतर्संबंध से है। इसी तरह अलग-अलग रंगों की चीर प्रकृति के विभिन्न रंगों की खुशहाली का प्रतीक है। प्रत्येक घर से चीर का टुकड़ा आना सामूहिकता का द्योतक है। इस चीर को टीके के दिन उतारकर इसे हर परिवार को देने की परंपरा भी है। चीर एक तरह से धार्मिक अनुष्ठान से अभिसिंचित होकर लोगों के लिए सौहार्द, भाई चारे और सामूहिकता का प्रतीक है। वहीं चीर के साथ ही कई क्षेत्रों और गांवों में होली के अवसर पर निशाण पूजने की परंपरा है। निशाण किसी राजा या वंशों का चिह्न या झंडा होता है, जो उनकी पहचान और क्षेत्र को दर्शाता है।