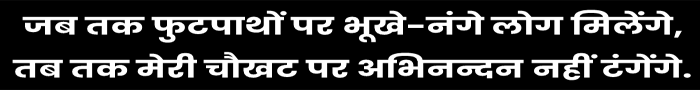आदर्श चौहान
भला कौन भूला होगा, जब डेढ़ दशक पहले जैसे स्कूटर पर करोड़ों के पत्थर जयपुर व जोधपुर आदि शहरों से लखनऊ लाए गए थे सुंदरीकरण के लिए? उसी तरह आजकल गायों के लिए कमोबेश प्रदेश के हर जिले में स्कूटर पर लाखों का हरा चारा व भूसा ढोया जा रहा है। इन हालात में ही कहा जाता है कि इंसान का पेट है या भैंस की नांद, जो भरने का नाम ही नहीं लेता है।
अधिकारी जब खाने पर आता है तो भैंस का चारा तक नहीं छोड़ता है। पेट है या भैंस की नांद, ऐसा उदाहरण अतीत के बिहार में देखा जा चुका है। उसी चारे की तरह आजकल उत्तर प्रदेश में गाय का चारा भी हर माह सुर्खियां बटोर रहा है। भला कौन भूला होगा, जब डेढ़ दशक पहले जैसे स्कूटर पर करोड़ों के पत्थर जयपुर व जोधपुर आदि शहरों से लखनऊ लाए गए थे सुंदरीकरण के लिए? उसी तरह आजकल गायों के लिए कमोबेश प्रदेश के हर जिले में स्कूटर पर लाखों का हरा चारा व भूसा ढोया जा रहा है। इन हालात में ही कहा जाता है कि इंसान का पेट है या भैंस की नांद, जो भरने का नाम ही नहीं लेता है।
एक आईएएस अधिकारी को वरिष्ठता के हिसाब से डेढ़ से साढ़े तीन लाख रुपए तक प्रतिमाह वेतन मिलता है और ढेरों सुविधाएं अलग से। जिलाधिकारी को तो तीन कारों सहित दर्जन भर लोगों की फौज सेवा के लिए मिलती है। इसके बावजूद घर बैठी पत्नियां उन्हें रास नहीं आतीं। कहीं न कहीं उनकी व्यवस्था जिलों से लेकर राजधानी तक करवा ही देते हैं। अगर सिर्फ दो दशक की बात करें तो दर्जनों ऐसे अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लाभ के पद पर पत्नी को बैठाने में प्रभाव का इस्तेमाल किया है।
स्कूलों में शिक्षक के नाम पर प्रशासनिक पद, एनजीओ और पद और कद के दबाव के चलते निजी सेक्टर (गैर सरकारी) में तो ऐसा सौ बार हो चुका है, पर सरकारी में होने लगे तो समझ लो कि हिप्पोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी व इडियोक्रेसी में बदल चुकी है ब्यूरोक्रेसी। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी नाम वाले होते हैं, जो नाम के पीछे कुछ भी करने (यू-ट्यूबर नहीं) के लिए तैयार हो जाते हैं। कई अधिकारियों ने ड्यूटी के दौरान मुश्तैदी पर जान तक गंवाई है हालिया दशकों में। जुझारूव नियम के पक्के लोगों का नाम लेने में न तो कोई बुराई है और न ही कोई संकोच होना चाहिए।
एक आईएएस हैं एम. देवराज, दुर्गा शक्ति नागपाल, अशोक खेमका, डॉ. राजू नारायण स्वामी, आर्म्सट्रांग पाम, अरुणा सुंदरराजन, स्मिता सबरवाल, दिव्या मित्तल, ऋतु माहेश्वरी, कृतिका ज्योत्सना व आंजनेय कुमार सिंह आदि, जिनकी सख्ती व ईमानदारी प्रदेश की सीमाओं से परे है। कुछ अन्य भी हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं, जो शुरू में बढ़िया चले, नाम को खूब उठाया, पर बाद में ट्रैक बदल दिया। यानी कि उनके नाम सूची से बाहर हो गए। दरअसल नाम बनाने में बड़ा वक्त लगता है और बिगड़ने में चंद मिनट। कोई भी एक गलती काफी होती है औरे को अर्श से फर्श पर लाने के लिए।
बदबू अगर हवा के रुख के साथ सरहद भी पार कर जाती है तो खुशबू भी चारों तरफ अपने आप फैलती रहती है, उसे तो हवा के साथ बहने की भी जरूरत नहीं होती। दृष्टांत के लिए मृग कस्तूरी, इत्र और फूलों में चंपा, चमेली, मोगरा, गेंदा, गुलाब व रातरानी आदि। उक्त लोगों की खासियत है कि किसी से डरकर काम नहीं करते। उनका नारा है कि कर नहीं तो डर नहीं। काम सही है, तभी करेंगे, नहीं तो नहीं।
इतिहास गवाह है कि गलत रास्ते पर चलने वाले गर्दन व नजर नीचे करके ही बात करते हैं। सृजन (कृत्य) के कारण ही ऊंची रहती है इनकी गर्दन (सिर) व गर्जन (स्वर) आदि। ये लोग न सस्पेंशन से डरते हैं, न टेंशन से और न ही ट्रांसफर व ट्रांसफर करने वाले से। देवराज की खूबी के कारण ही पीठ के पीछे मातहत यमराज तक कह डालते हैं। उन्नाव का जिलाधिकारी रहते हुए एक बार उनकी पत्नी सरकारी गाड़ी से बाजार में दिख गई थीं तो ड्राइवर को फटकार लगाते हुए गाड़ी ले ली थी और पत्नी को रिक्शे से घर भेजा था।
अतीत में लाभ के पद को लेकर प्रदेश से लेकर देश तक कई बार काफी हल्ला-हंगामा मच चुका है और बात हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक गई है। बार-बार नार्म्स सेट करने के बाद भी थोड़े से अंतराल के बाद ही चीजें फिर वीभत्स हो जातीहैं और अपने रूप में सतह पर आ जाती हैं। ऐसा अतिरिक्त बेशर्मी के कारण भी हो सकता है और कमाई के कारण भी। यही हालात देखकर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अधिकारियों की पत्नी पदेन पद पर क्यों? अंग्रेजों के औपनिवेशिक दौर की इस प्रथा को खत्म किया जाए।
एक हालिया आदेश में कोर्ट ने प्रदेश की सहकारी समितियों में मुख्य सचिवों और जिलाधिकारियों जैसे शीर्ष नौकरशाहों की पत्नियों के पदेन पदों पर रहने की स्थिति पर न सिर्फ आपत्ति जताई है, बल्कि कटाक्ष करते हुए जमकर फटकार भी लगाई है। साथ ही राज्य सरकार से कहा है कि वह नियमों में संशोधन कर इस औपनिवेशिक मानसिकता दर्शाने वाली प्रथा समाप्त करें। न्यायमूर्ति सूर्यकांत व उज्ज्वल भुइया की पीठ ने सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज के इस कथन पर भी आपत्ति जताई कि समितियों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि समिति-सोसाइटी के लिए अब आदर्श नियम बनाने होंगे। अदालत ने कहा कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत जिन सोसायटी को प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ दिया गया था, उन्हें सरकार द्वारा लागू कर आदर्श नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का पालन न करने पर सोसायटी वैधानिक दर्जा खो देगी। गौरतलब है कि पीठ बुलंदशहर की 1957 से कार्यरत जिला महिला समिति से संबंधित विवाद की सुनवाई कर रही थी। मामले में प्रशासन ने महिलाओं के कल्याण के लिए नजूल भूमि दे दी थी।
मूल उपनियमों के अनुसार बुलंदशहर के कार्यवाहक डीएम की पत्नी को महिला समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करना जरूरी था। समिति ने साल 2022 में उपनियमों में संशोधन करने का प्रयास किया, जिससे डीएम की पत्नी को समिति का संरक्षक बना दिया। राज्य हाईकोर्ट से पक्ष में फैसला न आने के बाद समिति ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि समिति काम करती रहे, लेकिन डीएम की पत्नी को सहकारी समिति का पदाधिकारी बनने व कामकाज में दखल से रोका जाए।
पीठ ने याचिकाकर्ता समिति को निर्देश दिया कि वह नजूल भूमि या अन्य संपत्ति पर कोई भी अतिक्रमण या तीसरे पक्ष के अधिकार का सृजन न करे, जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसे सौंपी गई हों। उल्लेखनीय है कि उक्त समस्या के तीन निकट संबंधी और सहयोगी और भी हैं। एक लाभ के पद, दूसरा हितों का टकराव और तीसरा- एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत। संक्षेप में इन पर भी रोशनी डालने के बाद ही बात पूरी हो सकेगी। 1996 से 98 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वयोवृद्ध नेता सीताराम केसरी ने इसे लेकर न सिर्फ सवाल खड़ा किया था, बल्कि सोनिया गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी लड़े थे।
उनका भी यही कहना था कि एक कद (व्यक्ति) को एक पद। नारायण दत्त तिवारी, शरद पंवार, पीए संगमा, ममता बनर्जी और जितिन प्रसाद का भी यही कहना रहा है। कुछ ऐसे ही विषयों को लेकर उक्त लोगों ने कांग्रेस को आंखें भी दिखाई थीं। 2022 में अशोक गहलोत के एक बयान कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की जरूरत नहीं है पर राहुल गांधी ने भी इच्छा प्रकट की थी कि एक व्यक्ति एक पद। कहने को भाजपा काडर बेस्ड पार्टी है और नियम-कानून का बड़ा ध्यान रखती है, पर आंतरिक संविधान की रोज ही हत्या हो रही है। किसी को मंत्री बना दिया जाता है, फिर भी वह संगठन का पद नहीं छोड़ता है।
विधायकों ने अपनी पत्नी, बच्चों, भाई व मां को ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक किसी न किसी पद पर बैठा रखा है और एक पद एक व्यक्ति का पद दशकों से हड़ताल पर है। प्रदेश के एक मंत्री ने अपने साले को मनोनयन के जरिए अपने विभाग में बड़ा पद दिया था तो सत्ता के गलियारों में काफी हंगामा हुआ था। पंजाब से शुरू हुई परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब अपने 20 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने का फैसला लिया था तो अदालत ने इसे लाभ का पद बताते हुए सभी की सदस्यता ही खत्म कर दी थी।
इसी तरह बीते दो दशकों में कई बीसीसीआई में हितों के टकराव का मुद्दा कम से कम दो बार उठ चुका है। हालिया मामले में संजीव गुप्ता ने बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी के खिलाफ हितों के टकराव की शिकायत में कहा था कि उनकी बहू मयंती लैंगर स्टार स्पोर्ट्स चैनल के लिएएंकरिंग करती हैं और स्टार स्पोर्ट्स के पास घरेलू सत्र के मीडिया अधिकार हैं। हालांकि बाद में यह शिकायत खारिज कर दी गई थी। एक बार सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, विराट कोहली और नीता अंबानी भी इसी पचड़े में फंस चुके हैं।
कमोबेश सभी खेल संघों पर नेता, आईएएस या आईपीएस के शिकंजे में हैं। इसी प्रकार राजकोष से दो पेंशन के मुद्दे का भी देशहित में अंत होना चाहिए। कोई कितने भी सरकारी विभागों में नौकरी कर ले या जनप्रतिनिधि बन जाए, पर पेंशन एक ही मिले क्योंकि निजी सेक्टर को छोडकर सारी पेंशन आती तो राजकोष से ही है। जनहित के ऐसे मुद्दों पर भी सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कोई टैक्स मनमानी करने व रेवड़ी बांटने के लिए नहीं देता है। राजनीति में अंधों द्वारा रेवड़ी बांटने की परंपरा काफी पुरानी है।
गौरतलब है कि प्रबुद्ध वर्ग ने इसकी आलोचना की थी, क्योंकि पैसा भले ही यूजीसी के जरिये आता हो, पर आता तो राजकोष से ही है। इससे पहले भी एक साथ दो जगह से वेतन या भत्ते लेने की कड़ी निंदा होती रही है कई मामलों में। उक्त वर्ग तो तब भी आपत्ति करता रहा है, जब कोई नेता या अधिकारी बीसीसीआई या अन्य खेल संघों में पदेन पद (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव) धारण करता है। सीधा सा अर्थ है कि जो कुछ बन गया है, वह दूसरों के हक पर भी डाका डालने में जुटा हुआ है। वह सब कुछ जुटा लेना चाहता है अगली से अगली पीढ़ी के लिए।
कुछ छोड़ना ही नहीं चाहता है दूसरों के करने के लिए। एक पद है तो दूसरे से दूर नहीं रह पा रहा है। वह भूलना चाहता है कि पद कम हैं और आवेदक आदमी ज्यादा। गौरतलब है कि लाभ के पद विधेयक को 2006 में पारित किया गया था,पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने पहले इसे आपत्तियों के साथ संप्रग सरकार को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। उनका कहना था कि कौन से पद लाभ के पद की परिधि में आते हैं, इसे तय करते वक्त निष्पक्षता का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही केंद्र द्वारा पारित यह विधेयक सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में समान और पारदर्शी तरीके से लागू हो।
ज्ञात हो कि जया बच्चन की सांसदी जाने के बाद प्याले में तूफान उठा था और सपा की गंभीर आपत्ति पर सोनिया गांधी ने न सिर्फ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था, बल्कि सांसदी से भी इस्तीफा दे दिया था और फिर से चुनाव जीतकर संसद पहुंची थीं। वर्तमान सरकार 65 साल पुराने इस कानून को खत्म कर नया कानून लाना चाहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व गवर्नर कलराज मिश्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने नए कानून की सिफारिश की थी। ज्ञात हो कि सबसे पहले लाभ के पद कामामला सुप्रीम कोर्ट ने 1964 में आया था।
याद होगा कि बीते दशक में लाभ के पद को लेकर बीसीसीआई में काफी बवाल हुआ था। इसी हफ्ते की बात करें तो असम के नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि राज्य के महाधिवक्ता देवजीत लोन सैकिया ने बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव और आईसीसी निदेशक की भूमिका निभाकर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। हालांकि जवाब में दोनों पदों को मानद बताया गया है, पर प्रबुद्धों का कहना है कि एक आदमी एक पद का सिद्धांत शातिर चालबाजियों के कारण नहीं बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते दशकों में कई मामले प्रकाश में आए हैं, जब ब्यूरोक्रेट व डेमोक्रेट (सांसद-विधायक) क्या, कई बार सरकारें तक लाभ के पदों पर नियुक्ति का लोभ संवरण नहीं कर पाती हैं।
राजकोष से अपनों को रेवड़ी बांटने के क्रम में लगता है, कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। लाभ के पद का मतलब है ऐसा पद, जो उस पद पर बैठे व्यक्ति को कुछ वित्तीय लाभ या अन्य फायदा पहुंचाता है। यह एक ऐसा शब्द है,जिसका इस्तेमाल कई राष्ट्र के संविधानों में कार्यकारी नियुक्तियों के लिए किया जाता है। कई देश विधायिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखने के साधन के रूप में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका के अधीन लाभ का पद स्वीकार करने से रोकते हैं।
हाल के साल में दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को राष्ट्रपति द्वारा अयोग्य करार दे दिया गया था। चुनाव आयोग द्वारा लाभ के पद के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सदस्यता रद्द करने की सिफारिश करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया था। मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अनुसार किसी भी विधायक द्वारा सरकार में ऐसे पद को नहीं धारण किया जा सकता है, जिसमें भत्ते, सुविधा एंव कोई शक्तियां मिलती हों।
इसके लिए विधानसभा से कानून पास किया जाता है और राज्यपाल, उप राज्यपाल या एलजी की मंजूरी भी चाहिए होती है, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया था। समाज के अहम वर्ग अर्ध सरकारी शिक्षकों को भी लेकर कुछ लोग नुक्ताचीनी करते रहे हैं कि वे बिना किसी कानूनी रोक के विधायक, मंत्री, सांसद, ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष तक बन सकते हैं। दूसरी ओर मंत्री व विधायक अपने बीवी-बच्चों को उक्त में से कई पदों पर आज भी बैठा रखे हैं। न कहीं नैतिकता का पालन किया जा रहा है और न ही कानून का।
संविधान में अनुच्छेद 102 (1) के अंतर्गत संसद सदस्यों के लिए तथा अनुच्छेद 191 (1) के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए ऐसे किसी भी लाभ के पद को धारण करने का निषेध किया गया है, जिससे उस पद के धारण करने वाले को किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता हो। अगर कोई विधायक किसी लाभ के पद पर आसीन पाया जाता है तो उसे अयोग्य करार देने के बाद सदस्यता जा सकती है। यह अवधारणा संसद व विधानसभा के सदस्यों की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखती है।
यह विधायिका को कार्यपालिका से किसी अनुग्रह या लाभ प्राप्त करने से रोकती है। साथ ही विधायी कार्यों व विभिन्न पद के कर्तव्यों में होने वाले टकराव को रोकती है। चूंकि लाभ के पद के संदर्भ में भारत में कोई स्थापित प्रक्रिया मौजूद नहीं है। अतः ऐसे में न्यायालय की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। गोविंद बसु बनाम शंकरी प्रसाद मामले में गठित संविधान पीठ ने लाभ के पद के संदर्भ में कई कारक निर्धारित किए हैं। जैसे- नियुक्तिकर्ता, पारितोषिक या लाभ निर्धारित करने वाला प्राधिकारी और पारितोषिक के स्रोत आदि।
अशोक भट्टाचार्य बनाम अजोय बिस्वास मामले में न्यायालय ने कहा था कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक मामले को उपयुक्त नियमों और अनुच्छेदों को ध्यान में रखकर ही निर्णय किया जाना चाहिए। स्पष्ट है कि लाभ के पद के संदर्भ में न्यायालय की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर भी सुस्पष्ट नियम का अभाव देखा गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, संविधान में ये धारा रखने का उद्देश्य विधानसभा को किसी भी तरह के सरकारी दबाव से मुक्त रखना था।
क्योंकि अगर लाभ के पदों पर नियुक्त व्यक्ति विधानसभा का भी सदस्य होगा तो इससे निर्णयों के प्रभावित होने का अंदेशा बना रहता है। सर्वविदित है कि भारत का संविधान दुनिया के बाकी बड़े देशों की तुलना में सबसे बाद में रचा गया है तो दुनिया के कई देशों के संविधान से विधान लिए गए हैं। अनुच्छेद 102 (1) (ए) सांसद को ऐसा पद धारण करने से रोकता है, जो वित्तीय लाभ प्राप्त करने का अवसर देता हो। यह केंद्र व राज्य सरकार के अधीन किसी पद को संदर्भित करता है, जिसमें वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। उल्लंघन के दौरान प्राप्त लाभ की वास्तविक राशि का वर्गीकरण पर असर नहीं पड़ता है।
संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1950, 1951, 1953 और 1959 थे, जो कुछ पदों को लाभ के पदों के रूप में दर्ज होने से छूट देते थे। अधिनियम की धारा तीन के आधार पर कुछ कार्यालय धारकों को संसद सदस्य होने से अयोग्य नहीं ठहराते थे। कोई व्यक्ति लोकसभा से अयोग्य हो जाता है, यदि वह लाभ का पद धारण करता है, पर 56 ऐसे पद हैं, जिन्हें लाभ के पद नहीं माना जाएगा। 2006 में कानून में फिर संशोधन किया गया था। संविधान की धारा 44 (पअ) में प्रावधान है कि जो कोई भी क्राउन के अधीन लाभ का पद रखता है, वह संसद में बैठने या चुने जाने के अयोग्य है।
यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या के अधीन है। 2018 में विवादित रिटर्न न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए दो-भागीय परीक्षण शुरू किया कि कोई कार्यालय क्राउन के अधीन है या नहीं। कोई पद क्राउन के अधीन होता है यदि नियुक्ति राष्ट्रमंडल या किसी राज्य की कार्यकारी सरकार की इच्छा पर की जाती है, भले ही सरकार पदधारक के कार्यकाल या पारिश्रमिक को नियंत्रित न करती हो। यदि सरकार पद धारण करने या उससे लाभ कमाने पर प्रभावी नियंत्रण रखती है तो। यूएसए में दो परिस्थितियों में कांग्रेस के किसी सदस्य को कार्यकारी पद पर नियुक्त होने से रोकने का विधान है।
कोई सीनेटर या प्रतिनिधि, जिस अवधि के लिए निर्वाचित हुआ है, किसी भी सिविल कार्यालय में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो उस अवधि के दौरान सृजित किया गया हो या जिसके वेतन में वृद्धि की गई हो और अमेरिका के अधीन कोई भी कार्यालय धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने पद पर बने रहने के दौरान किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। महाभियोग के मामलों में निर्णय पद से हटाने तथा सम्मान, विश्वास या लाभ के किसी भी पद को धारण करने और उसका आनंद लेने के लिए अयोग्य ठहराने से आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन दोषी ठहराया गया पक्ष फिर भी कानून के अनुसार अभियोग, परीक्षण, निर्णय और दंड के लिए उत्तरदायी होगा।
दूसरा, ट्रस्ट या लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति कांग्रेस की सहमति से विदेशी शक्तियों से उपहार, पारिश्रमिक, पद या उपाधि प्राप्त कर सकता है। तीसरा, किसी व्यक्ति के पास ट्रस्ट या लाभ का पद हो, उसे राष्ट्रपति के निर्वाचक के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है।
सहायक प्रोफेसर होना, लाभ का पद नहीं
सांसद के विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत होने को लाभ के पद के दायरे में नहीं माना गया है। एसोसिएट प्रोफेसर पद को सांसद के कर्तव्य का पालन करने के दौरान हितों का टकराव नहीं माना जाएगा। इस पद को केंद्र व राज्य सरकार के सीधे अधीन नहीं माना गया है। इस तरह आजादी के बाद ही सहायक प्रोफेसर पद को लेकर बड़े नेताओं के बीच लाभ के पद की व्याख्या को लेकर चलती रही बहस पर पहली बार विराम लग गया है। पश्चिम बंगाल के बोलपुर से सांसद व विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के सहायक प्रोफेसर डॉ. अनुपम हाजरा के प्रकरण में राजस्थान के सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली लाभ के पदों संबंधी संसद की संयुक्त समिति ने अनुशंसा में सहायक प्रोफेसर के पद को लाभ का पद नहीं माना है।
समिति ने प्रोफेसर के पद पर किसी सांसद के कार्यरत रहने को कानूनी अड़चन नहीं माना है। लाभ के पद की यह नजीर प्रदेश के विधायकों के मामलों में भी संसदीय परंपरा एवं विधान के तहत भविष्य में ऐसे विवाद होने पर गाइडलाइन बन गई है। सामने आया कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की पात्रता के दौरान एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी लाभ के पद की व्याख्या के लिहाज से सरकार से लाभ नहीं लेने की परिपाटी के दायरे में ही आता है। पड़ताल के बाद गोपनीय रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को भेज दी है।
विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा नहीं, बल्कि परिनियमों के तहत एक्जीक्यूटिव काउंसिल के जरिए की जाती है। सहायक प्रोफेसर का पद सांसद बनने में बाधक नहीं माना जा सकता। यह पद केंद्र-राज्य के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है। सहायक प्रोफेसर को दूसरी सरकारी नौकरी जैसा नहीं माना जा सकता है। शिक्षण के बदले वेतन प्राप्त करना सरकार से लाभ लेने जैसा नहीं। वेतन एवं भत्ते विश्वविद्यालय के निधि से मिलता है, न कि सरकार से।
प्रसंगवश बता दें कि कानून में एक और बड़ा गड्ढा छोड़ा गया है नीति नियंताओं द्वारा कि लोग 55 साल में भी विश्वविद्यालयों के उप कुलपति बन जा रहे हैं और वहां से रिटायर होकर फिर पुराने संस्थान में पढाने लगते हैं। नैतिकता का घोर उल्लंघन है यह नियम तो यह होना चाहिए कि रिटायरमेंट के तीन साल पहले ही वीसी बनाया जा सकेगा ताकि छुट्टी के बाद सीधे घर या शोध संस्थान या कहीं अन्यत्र मनोनयन हो, न कि पुराने संस्थान में जाकर पढ़ाना। वैसे तो किसी भी उम्र में पढ़ाना गलत नहीं हो सकता, पर यह नैतिक रूप से पुराने साथियों को असमंजस में डालने वाला बिंदु है।