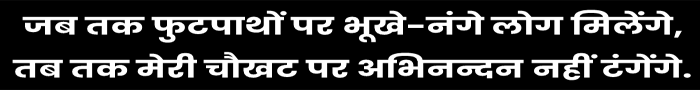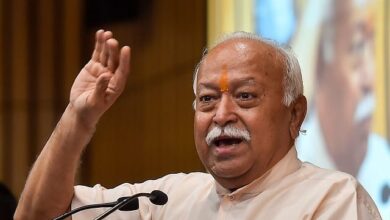शिल्पा सिंह
वायु व जल प्रदूषण की तरह ध्वनि प्रदूषण भी आदमी का दुश्मन होता है। इसे स्लो प्वॉइजन कहना ज्यादा ठीक रहेगा। यह हर क्षण सेहत पर प्रतिकूल असर डालता है। नई रिपोर्ट में भी कहा गया है कि उक्त कारणों से लखनऊ जैसे शहर में लोगों की औसत आयु पांच साल से ज्यादा घट गई है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मेगा लांचिंग का मकसद यही था कि देश और प्रदेशवासियों को ध्वनि और वायु प्रदूषण से राहत दी जा सके। साउंडलेस होने के कारण भारी राहत भी है। यह दीगर बात है कि साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। शहर भर गए हैं, सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं बची है। छोटे-बड़े किसी भी शहर में घुसने के लिए बड़ा कलेजा होना चाहिए। वाहन दिन भर रेंग रहे हैं। इंजन की आवाजों के बाद हॉर्न कान फोड़े हैं।
चौराहों व सड़कों के किनारे का जीवन दुरूह हो गया है। मानकों की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन 65 डेसीबल से ज्यादा के शोर को ध्वनि प्रदूषण मानता है। यह जैसे-जैसे बढ़त्ता जाता है और सौ के ऊपर पहुंचता है तो मानव जीवन को परेशानी में डालने वाला होता है। बता दें कि आमतौर पर आदमी का काम 20-30 डेसीबल से चल जाता है। रॉक कंसर्ट, शोर करने वाली बड़ी मशीनों व लाउडस्पीकर आदि से मुख्य तौर पर ध्वनि प्रदूषण होता है। देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि दूसरे की जगह खुद को रखकर देखें। उसके बाद ही वक्तव्य जारी करें।
वॉल्यूम चाहे खुद का हो, गाड़ी मोटर के इंजन का हो या फिर लाउडस्पीकर का, बस उतना ही बढ़ाने की आजादी है, जितने की शिकायत न करनी पड़े। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, मशीनों का नियमित रख-रखाव करें और जहां तक संभव हो ईयर फोन का इस्तेमाल करें। फिलवक्त हाल ऐसा है कि तहजीब के लिए मुद्दत से मशहूर रहे कई शहर बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। इसके लिए जिम्मेदार है जरूरत से ज्यादा आबादी बढ़ाने की आजादी। इस समय आबादी और संतुलित वाहन नीति न होने के कारण चीजें गड्ड-मड्ड हो गई हैं, जिसके कारण संतुलन बिगड़ने से प्रकृति भी नाराज सी लगने लगी है।
आज के परिवेश में एक बात गले के नीचे नहीं उतरती है कि जनमानस ने भांग खाली है या कुएं में ही भांग गिर पड़ी है या यूरिया व डीएपी खाद के जरिए शरीर से लेकर खोपड़ी तक में गर्मी इतनी भर चुकी है कि नियम और कानून बौने लगने लगे हैं या फिर पुलिस व प्रशासन के बुलंद इकबाल का सामाजिक पारिवारिक संबंधों की तरह बोनसाईकरण हो गया है। कायदे का एक दरोगा हो देश के हर शहर के हर थाने में तो शहरी बहुत कायदे में रहेंगे व अनुशासित एवं सभ्य नागरिक भी फायदे में? चूंकि पुलिस कार्यपालिका का हिस्सा है इसलिए सभी कानूनों के क्रियान्वयन की बड़ी जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर रही है सदा से। फिर चाहे कानून विधायिका में बना हो या न्यायपालिका (निर्देश) में। दोनों को लागू करने का काम पुलिस ही करती है।
गांवों से लेकर शहरों तक अराजकता का आलम ये है कि डंडे के बिना पीठ की जकड़न जाती नहीं लगती। हर शहर के चौराहों पर दोपहिये पर तीन युवा बैठे आमतौर पर मिल जाएंगे तो तीन पहिये पर छह। बिना हेलमेट के चौराहा पार करने में चंद साल पहले तक कांप जाते थे, पर अब वह भी जाता रहा। किसी चौराहे के 50 कदम आगे-पीछे दोपहिया वाहन पर तीन छोड़िए, चार और पांच तक बैठे मिल जाएंगे, जिससे लगता है कि कानून की किताब के पन्ने और पुलिस के डंडे का खौफ उनके दिल से ऐसे निकल भागा है, जैसे गधे के सिर से सींग। यही हाल धार्मिक स्थलों पर टांगे गए चार-चार लाउडस्पीकर का भी है।

यह मामला सिर्फ ध्वनि प्रदूषण का न होकर अराजकता, संवैधानिक स्वतंत्रता का है व धार्मिक प्रतियोगिता का भी। अतीत में ज्यादा खाद-पानी पा गए एक हुजूम ने 50 फुट ऊंची दीवार पर चार-छह लाउडस्पीकर बांध दिए और जिसके पास मीनार नहीं थी, उसने चंदा लगाकर प्रत्युत्तर में 51 फुट ऊंचे बांस पर दो-तीन बांध दिए। सवाल है कि कोई वह सब क्यों सुने और क्यों सुनाया जाए, जिससे दूर-दूर तक उसका कोई लेना-देना नहीं है और सौहार्द्र के बजाय विद्वेष फैला रहा है? गर्मी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डा, चारबाग, दुबग्गा, चौक, ऐशबाग, नक्खास, निशातगंज, आलमनगर, अमीनाबाद, बाजारखाला, याहियागंज, काशवाणी के आगे-पीछे की मस्जिद से कोर्ट के आदेश के बाद और योगी 1.0 में भी लाउडस्पीकर नहीं उतारे जा सके थे।
इस मुद्दे पर पूरे देश व प्रदेश का हालत करीबन एक जैसा है। हर शख्स परेशान सा है और हालात के मद्देनजर कई मामलों में चीन जैसी कार्रवाई की अपेक्षा करने लगा है। इस तरह ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम कागजी साबित हुई है, क्योंकि एक ओर से लाउडस्पीकर उतरवाए जाते हैं तो दूसरी ओर से टंगने शुरू हो जाते हैं इसीलिए न्यायपालिका, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और मुख्यमंत्री को दोबारा डांट-फटकार का सहारा लेना पड़ा। हाल के साल में यह मुद्दा तब और गर्म हुआ, जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने चेतावनी जारी की, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई और पूरे प्रदेश से हजारों लाउडस्पीकर उतारे गए थे। कुछ हैं, जिन्हें वही सब पसंद है, जो बहुतायत देशवासी पसंद नहीं करते या दिक्कत महसूस करते हैं। कुल मिलाकर मामला धार्मिक कम और मतभेद के बाद मनभेद के चलते चिढ़ा-चिढ़ी का ज्यादा लगता है।
इससे पहले बॉलीवुड सिंगर व अभिनेता सोनू निगम ने कहा था कि प्रायः हम लोग देर रात तक काम करते हैं और भोर में शोर से नींद खराब हो जाती है, जबकि आराम पर सबकी तरह हमारा भी हक है। सर्वाधिक दिक्कत रमजान में होती है, जब आधी रात के बाद से ही चिल्ला-चिल्ला कर मौलवी बताना शुरू करता है कि रात के दो बज गए हैं, जाग जाओ। मस्जिद की घड़ी में भोर के ढाई बजे हैं, हाथ मुंह धो लो। अब तीन बजे हैं सहरी का वक्त हो गया है। ये सब क्या है? रोजा रखा है सौ ने और परेशान हो रहा है 10000 की आबादी वाला पूरा गांव या किसी शहर का पूरा मोहल्ला।
जागना या सोते रहना, कुछ जिम्मेदारी निभाना उसका भी फर्ज है, जिसे रोजा रखना है या सारी जिम्मेदारी बेचारा लाउडस्पीकर ही उठाएगा। उस बेचारे पर इतना काम डाल दिया कुछ अहमकों ने कि पूरा देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया और बाकी मजहब, धर्म व पंथ उसके पीछे पड़ गए हैं। यूपी से होते हुए लाउडस्पीकर विरोधी लहर एमपी होते हुए राजस्थान जा पहुंची और चारों राज्यों में करीब एक लाख लाउडस्पीकर उतारने व इतने की ही आवाज कम करने की खबरें आ रही हैं, पर सबसे बड़ी गफलत यहीं पर है, जब दारोगा कहता है कि आवाज कम करवा दी गई है।
कोर्ट का आदेश क्या है आवाज कम करने का या लाउडस्पीकर उतारने का क्योंकि कितने दिन तक आवाज कम रहेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? दरोगा के मौके से हटते ही कोई अहमक या जाहिल कितने मिनट तक लाउडस्पीकर की आवाज पर काबू रखेगा और कितने मिनट तक नहीं बढ़ाएगा, इसकी गारंटी संबंधित क्षेत्र का थाना या चौकी प्रभारी लेगा? ज्ञात हो कि पीलीभीत के मुख्तियार अहमद ने यूपी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मस्जिद पर फिर से लाउडस्पीकर बांधने की इजाजत मांगी थी। इस पर कोर्ट ने फैसले में कहा था कि धार्मिक या पूजा स्थल ईश्वर की प्रार्थना के लिए होते हैं। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल धार्मिक प्रोग्राम का न तो हिस्सा है और न ही अधिकार।
मतलब साफ है कि यदि बिना होंठ खोले मन में कही हुई बात भी ईश्वर सुन लेते हैं तो फिर लाउडस्पीकर से बताने-सुनाने की जरूरत क्यों? सभी को शांति से जीने की संविधान प्रदत्त आजादी है। पूरे 600 साल पहले संत कबीरदास जी द्वारा साखी के तहत लिखे गए एक दोहे से पूरी कथा का पटाक्षेप हो जाएगा, …ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाय। यानी कि दिलों में जो श्रद्धा है, वह किसी लाउडस्पीकर, बांग या चिल्लाने की मोहताज नहीं है। चिल्लाने से श्रद्धा बढ़ती है, इस बात का मानवता के 5000 साल के इतिहास में कोई प्रमाण नहीं हैं। उक्त फैसले के बाद योगी 1.0 में हजारों लाउडस्पीकर उतारे गए थे। एक-एक मीनार से चार से छह तक उतारे गए थे, जो दोबारा बांध दिए गए।
इस मानसिकता और इन हालात के बाद आवाज कम करवा दी गई है, यह बोलकर कौन जाहिल करोड़ों लोगों को भ्रमित कर रहा है? इस तरह काम चलाने वाले के लिए सलाह है कि ऊंचाई प्रतिबंधित कराने पर ध्यान दे। जरूरत के समय सिर्फ जमीन पर रखे जा सकेंगे साउंड बॉस और उसकी आवाज की भी शिकायत करने पर जब्त किए जा सकेंगे। यहां सवाल यह है कि हालात फिर से इतने बेकाबू क्यों हो गए कि योगी 2.0 में सीएम ऑफिस को ट्वीट करके पुलिस को हाईकोर्ट के निर्देश की याद दिलानी पड़ी। हाल ही में की गई पोस्ट में कहा गया था कि धर्मस्थलों व गीत-संगीत के कार्यक्रमों में तय मानक से ज्यादा आवाज व निर्धारित समय के बाद लाउडस्पीकर व डीजे उत्तर प्रदेश में न बजें। कानफोडू स्वर वृद्धों, रोगियों, विद्यार्थियों व प्रतियोगी छात्रों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं।
पूर्व में प्रभावी कार्रवाई हुई थी, फिर निरीक्षण की जरूरत है, जहां भी मिलें तत्काल उतारे जाएं। कोर्ट के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों से 37,000 से अधिक लाउडस्पीकर हटाए गए हैं तो 55,000 की आवाज कम कर दी गई। ट्वीट को जिन जिलों ने सर्वाधिक गंभीरता से लिया, उनमें अव्वल रहा फिरोजाबाद, जहां के प्रशासन ने आनन-फानन अभियान चलाकर 13 थाना क्षेत्रों में ड्रोन से सर्वे कराया। नोटिंग हुई व तुरंत एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को जो भी गैर कानूनी है, उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए। जिले में हड़कंप मचना तो इसके बाद तय था। लोग अपने-अपने लाउडस्पीकर उतारने में जुट गए, जो यह सोच रहे थे कि प्रशासन उनकी मस्जिद तक नहीं पहुंचेगा, गलत थे और एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर लाउडस्पीकर को हटवाया।
इसी प्रकार शांति व्यवस्था और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन ने थाना सिविल लाइंस, क्वार्सी और जवां क्षेत्र में धार्मिक स्थलों से 68 लाउडस्पीकर उतरवाए हैं व चेतावनी के साथ 57 की आवाज को कम कराया है। शांति समिति की बैठक में क्षेत्र के धर्मगुरु, डिजिटल वालंटियर, ग्राम प्रधान और ग्राम प्रहरी से अधिक से अधिक सीसीटीवी लगवाने की अपील की? इससे पहले पुलिस ने धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर की ध्वनि का जायजा लिया था और मानक से ज्यादा जहां-जहां आवाज पाई गई थी, वहां-वहां कार्रवाई की गई। कई ऐसी जगह थीं, जहां बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगे हुए थे, उन्हें उत्तरवा दिया गया था। हालांकि बड़ी आबादी का कहना है कि प्रदेश के साथ पूरे जिले में सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
आधे जिले में कार्रवाई आधे इंसाफ की तरह है। माना कि बड़ा इलाका शहरी ही है पर देहात में रंजिश बढ़ रही है, जिस पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। शिकायत यह भी है कि दुल-मुल रवैये के कारण पुलिस के जाते ही जाहिल आवाज बढ़ा देते हैं। बता दें, प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए लाउडस्पीकर बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसके मद्देनजर पीछे भी कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इसमें पीस कमेटी की भी मदद ली गई है। कोर्ट ने आवाज के लिए जो मानक तय किए हैं, उनका पालन सभी के लिए जरूरी है। आवाज धार्मिक स्थलों के कैंपस के अंदर ही रहे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती।
वहीं जौनपुर के एसपी ने दो कदम आगे जाकर आधी रात को ही सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थलों से अवैध और मानक से ज्यादा आवाज वाले लाउडस्पीकर उतरवाने शुरू कर दिए थे। पुलिस ने शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए शहर में जांच की और निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी भी दी। कोर्ट के आदेशों के मद्देनजर कन्नौज के सिकंदरपुर चौकी प्रभारी ने पुलिस बल के साथ धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए। बिना परमिशन के चल रहे लाउडस्पीकर पर दृढ़ता से कार्रवाई की गई। उधर, पीलीभीत में जिले भर में पुलिस ने लाउडस्पीकर उतरवाने का अभियान चलाया। 133 धार्मिक स्थलों से तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर उत्तरवाते हुए स्कूलों व मरदसों के संचालकों को चेतावनी दी गई।
इस बीच, फिरोजाबाद पुलिस ने बोर्ड एग्जाम को देखते हुए घनी आबादी में बनी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए हैं। थाना रामगढ़ इलाके में ध्वनि प्रदूषण को लेकर चलाए गए अभियान के तहत एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ व थाना पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की अपील की और मस्जिदों पर बड़ी संख्या में लगे लाउडस्पीकर को उत्तरवा कर रखवा दिया। अभियान में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। लाउडस्पीकर स्वयं उतार कर रखने लगे। थाना क्षेत्र में बने बैंक्विट हाल व अन्य स्थानों पर भी पुलिस ने ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाद्य यंत्रों को तेज आवाज में न बजाने का निर्देश दिया।
पहले भी अभियान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चलाया जा चुका है, पर पूरे प्रदेश की परेशानी की बात यही है कि सहयोग नहीं मिल रहा है। जैसे ही पुलिस मौके से हटती है तो लोग अगले ही दिन फिर टांग देते हैं। एसपी सिटी ने कहा कि घनी आबादी क्षेत्र में तेज आवाज में बजाये जा रहे लाउडस्पीकर और अन्य वाद्य यंत्रों पर पुलिस की नजर लगातार रहेगी। शिकायत पर उपयोगकर्ता के विरुद्ध त्वरित व विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर, टूंडला सर्किल में भी उक्त आशय का अभियान चलाया गया। पुलिस ने नगला सहित शहर की पांच मस्जिदों से ध्वनि विस्तारक यंत्र चेतावनी के साथ उतरवाए। मंदिरों में भी मानक के अनुसार बजाने के निर्देश दिए। मंदिर की शिकायतें भी कम थीं, क्योंकि उनमें मीनार जैसा कुछ नहीं होता है, लिहाजा ध्वनि दूर तक नहीं जाती है।
विवाह स्थलों, धर्मशालाओं और मेला नुमाइश ग्राउंड में लाउडस्पीकर लगाने वालों को जागरूक करते हुए सतर्कता बरतने की अपील की गई। मुस्लिम समुदाय ने भी इस काम में सहयोग किया। पुलिस अधीक्षक नगर कहते हैं कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले लाउडस्पीकर परीक्षा काल में बच्चों के लिए काल हैं और उनका ध्यान भंग कर रहे हैं, सो सभी पक्ष एहतियात बरतें। यह अभियान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन के क्रम में करीब एक माह से चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2005 को ध्वनि प्रदूषण पर दिए गए अहम फैसले में कहा था कि देश के हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है, जो उसके जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।
कोर्ट ने साफ किया था कि लाउडस्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना भले अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के अंतर्गत आता हो, लेकिन यह किसी के जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सार्वजनिक स्थल पर रात 10 से सुबह छह बजे तक शोर करने वाले उपकरणों पर पाबंदी लगाई हुई है। तत्कालीन चीफ जस्टिस आरसी लाहोटी और जस्टिस अशोक भान की खंडपीठ ने उक्त आदेश दिया था। यह भी कहा था कि किसी को भी शोर मचाकर पड़ोसियों और आस-पास वालों के लिए परेशानी पैदा करने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोग अनुच्छेद 19 (1) ए में मिली अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन लाउडस्पीकर चालू कर कोई भी व्यक्ति इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने विस्तार से समझाया था कि अगर किसी के पास बोलने का अधिकार है तो दूसरे के पास नहीं सुनने का अधिकार है।
अगर किसी को जबरदस्ती तेज आवाज में लाउडस्पीकर सुनाया जाता है तो यह उसके शांति और आराम से प्रदूषणमुक्त जीवन जीने के अनुच्छेद 21 में तहत मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम नियम, 2000 के मुताबिक कामर्शियल, शांत और आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि तीव्रता की सीमा तय की गई है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिन में 75 और रात में 70 डेसीबल, कामर्शियल के लिए दिन में 65 और रात में 55 और आवासीय क्षेत्र के लिए दिन में 55 और रात में 45 तय की गई है।
2008 में मुंबई का नो हांकिंग डे
किसी भी प्रकार की अनुपयोगी ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, जिससे जीव-जंतुओं को परेशानी होती है। महानगरों के जीवन स्तर के हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शोर को कम करने के लिए दिल्ली ने 2022 में प्रेशर हॉर्न, संशोधित साइलेंसर और अत्यधिक हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर चालकों को दंडित भी किया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि बेंगलुरू पुलिस ने 2022 में 301 मस्जिदों, मंदिरों, चर्चों और अन्य संस्थानों को स्वीकार्य डेसीबल स्तरों के भीतर लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए नोटिस थमाई।
उत्तर प्रदेश के हालात देखकर लगता है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण अभी सरकार की प्राथमिकता में नहीं हैं। इसके विपरीत अमेरिका में 60 के दशक से ही यातायात शोर को रोकने पर काम शुरू हो गया था। 70 के दशक में लगाए गए पर्यावरण प्रतिबंधों ने प्रयासों को लोकप्रिय बना दिया। शोर अवरोधक ध्वनि दीवारें बनने लगी थीं, जब कि भारत में अब प्रयास गति पकड़ रहे हैं। किसी भी इंजन की गति शोर को बढ़ाती है। ट्रैफिक जाम की रफ्तार के कारण जहां गति और शोर कम हुआ है तो जाम में हॉर्न बजाने की बेहूदगी ने लोगों की परेशानी चार गुना तक बढ़ा दी है।
गंभीर मुद्दे पर मौन करता है परेशान
राजधानी लखनऊ में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए लखनऊ में कुल 10 रियल टाइम एंबिएंट नाइस मॉनीटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पांच स्टेशनों के दौरे में तीन मौन व दो औद्योगिक क्षेत्र शामिल थे। पांच अन्य मॉनीटरिंग स्टेशन पता करने पर अधिकारियों ने जगहों के बारे में कुछ नहीं बताया। तालकटोरा (औद्योगिक क्षेत्र), आईटी कॉलेज (मौन क्षेत्र) और एसजीपीजीआई (मौन) में स्थित मॉनीटरिंग नेटवर्क पेड़-पौधों की पत्तियों से ढक गए थे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओ एंड एम पार्टनर कंपनी एसजीएस वेदर की तकनीकी टीम से बात की गई तो उन्होंने बार-बार बचने की कोशिश की और कहा कि कैलिबरेशन और डिसेमिनेशन की जिम्मेदारी केंद्रीय बोर्ड की है।
उनका काम सिर्फ नेटवर्क स्थापित करना था और कोई जानकारी उनके पास नहीं है। बहुत खोजने पर करीब 550 एकड़ में फैले एसजीपीजीआई में भोजनालय के करीब 15 फीट ऊंचाई पर पत्तों से घिरा हुआ एक नॉइज मॉनीटरिंग नेटवर्क और लगभग आधा ढका हुआ माइक्रोफोन का सेंसर मिला था। आईटी कॉलेज क्षेत्र में जमीन पर चारों ओर से पत्तों से घिरा पूरा नेटवर्क और तीन ओर से नॉइज के माइक्रोफोन का सेंसर छिपा हुआ था। एक और बात, 10 में से एक नॉइज मॉनीटरिंग सिस्टम की एम्बेडेड एलईडी डिस्प्ले कई महीने से नेटवर्क की समस्या के कारण बंद पड़ी थी। साइलेंस जोन में दिन में 50 और रात 40 डेसीबल का मानक तय है, लेकिन आईटी कॉलेज के बाहर दिन के यातायात का शोर 80 के पार पहुंच जाता है।
तालकटोरा के औद्योगिक क्षेत्र में पार्क के कोने में जमीन पर पेड़ों के पत्तों से घिरा हुआ एक नॉइज मॉनीटरिंग स्टेशन दिखा। गार्ड ने बताया कि कोई आता होता तो मशीनें पत्तों से ढकी हुई नहीं, बल्कि साफ व ठीक मिलतीं। एसजीएस वेदर व सीपीसीबी की वेबसाइट में कहा गया है कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरू, लखनऊ व हैदराबाद में कुल 70 रियल टाइम ध्वनि प्रदूषण निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। सात शहरों के 70 स्टेशनों में एक भी जोन साइलेंस जोन के तहत नहीं दिखाई दिया, जबकि ध्वनि प्रदूषण विनियमन व नियंत्रण नियम 2000 के मुताबिक, 100 मीटर के तहत शिक्षण संस्थान, अस्पताल और कोर्ट परिसर के बाहर ध्वनि प्रदूषण पर पाबंदी है। सर्वर पर आईटी कॉलेज, एसजीपीजीआई व गोमती नगर का लोहिया हॉस्पिटल साइलेंस जोन भी हैं, पर आवासीय जोन नजर आते हैं।
ऐसा क्यों के सवाल पर यूपी प्रदूषण बोर्ड के सहायक वैज्ञानिक ने बताया कि इससे अवगत नहीं हैं। दिल्ली स्थित सीपीसीबी हेडक्वार्टर में बैठे वरिष्ठ वैज्ञानिक कहते हैं कि इस मुद्दे पर तो उनका या टीम का कभी ध्यान ही नहीं गया। वह इसे ठीक कराएंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से अध्ययन कर चुके उच्च न्यायालय के अधिवक्ता व विधि सलाहकार दुर्गेश कुमार शुक्ल सवाल करते हैं कि नगर निगम ने साइलेंस जोन होने पर बोर्ड क्यों नहीं लगाया? क्या ध्वनि प्रदूषण की दशा में बोर्ड या पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई की?
क्या एसपीसीबी ने इस बारे में कोई जागरूकता मुहिम चलाई? इस पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि वह मीडिया से बातचीत के लिए अधिकृत नहीं हैं, दिल्ली मुख्यालय ही कुछ बता सकता है। दिल्ली स्थित नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल (एनजीटी) प्रधान पीठ की वकील कहती हैं कि जमीनी स्थिति चिंताजनक है। कई ऐसे प्रोजेक्ट व विभाग हैं, जो व्यर्थ ही वेतन ले रहे हैं और बड़ा इनवेस्टमेंट खराब हो गया है। पर्यावरण मंत्रालय के सहयोगी सीपीसीबी और राज्य बोर्डों ने वायु और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम व व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के नाम पर मॉनीटरिंग स्टेशन लगाकर पैसा व्यर्थ बहा दिया।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या राष्ट्रीय हरित अधिकरण ये सभी अपने कार्य को बारीकी से अंजाम देते आए हैं, लेकिन आदेशों के बाद भी सीपीसीबी में बैठे कई अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। लखनऊ के 10 में से आठ स्थानों पर दर्शाए जा रहे आंकड़ें विचलित करते हैं। बाकी बचे दो क्षेत्र में से एक बोर्ड के लखनऊ मुख्यालय में है तो दूसरा औद्योगिक क्षेत्र चिनहट में। इन दोनों क्षेत्रों में लगा मीटर कई महीनों से बंद पड़ा है, जबकि मुख्य सर्वर पर आधा अधूरा आंकड़ा दर्ज हो रहा है। खास बात यह है कि यूपीपीसीबी के सदस्य सचिव सहित सभी आलाधिकारी यहां बैठते हैं, लेकिन उन्हें बंद पड़े मॉनीटरिंग स्टेशनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
मुख्य पर्यावरण अधिकारी को भी ई-मेल करके उक्त बातों का जवाब मांगा गया, यूपीपीसीबी और सीपीसीबी को भी टैग किया गया पर आदमी की सेहत जैसे गंभीर मुद्दे पर मौन परेशान करता है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 21 में बिना शोरगुल के शांति से रहने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत लखनऊ में ध्वनि प्रदूषण के आंकड़ों की निगरानी करने के लिए मॉनीटरिंग नेटवर्क, क्वॉलिटी सेंसर और माइक्रो फोन लगाए गए थे, लेकिन ये प्रयास जमीनी स्तर पर फेल हो गए हैं।
ध्वनि प्रदूषण : कलह की वजह
बात अगर सिर्फ वायु प्रदूषण की होती तो इसे मूक हत्यारा ही कहना सबसे बेहतर रहता, पर चूंकि मामला ध्वनि प्रदूषण का है तो इसे कई बीमारियों की वजह माना जा सकता है। यह भी कहना वाजिब होगा कि इससे उपजे तनाव, एनजाइटी, आक्रामकता, स्मृति लोप व चिड़चिड़ाहट घर से लेकर सड़क व दफ्तर तक कलह की वजह बनते हैं। कई संस्थाएं सर्वेक्षण आदि में लगी रहती हैं। एक संस्था के करीब 50 वालंटियरों ने 15 शहरों के शांत और आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की जांच की तो शोर का स्तर 50 डीबी की अनुमेय सीमा से लगभग 50 प्रतिशत अधिक पाया था।
कमोबेश सभी शहरों का हाल एक जैसा ही है। जैसे-जैसे विकास अभूत पूर्व गति पकड़ता है, वैसे-वैसे यातायात का शोर और अन्य प्रकार के ध्वनि प्रदूषण का स्तर बदतर होता जाता है, जिससे स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है। मकान निर्माण और ड्रिलिंग आदि का शोर भी परेशानी की वजह बन रहा है। कोरोना काल में चमत्कारिक रूप से ध्वनि और वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार देखने को मिला था। विशेषज्ञों की मानें तो ध्वनि प्रदूषण प्रजनन चक्र को भी बाधित करता है और प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो चला है।
देखने में आया है कि जंगली जानवर भी मानवीय गतिविधियां तेज होने पर ठिकाने बदल लेते हैं, क्योंकि अवांछित ध्वनि मानव के साथ पशु-पक्षी भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। हालांकि सभी शोर प्रदषण नहीं होते हैं। दिन के समय शोर का स्तर डीबी तक आराम से आदमी बर्दाश्त कर लेता है तो रात में 30 से अधिक नींद में बाधा डालता है। समय-समय पर इसमें भी सुधार होते रहते हैं। जैसे – 2018 में डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य कारणों से यातायात शोर को 53 डेसीबल तक सीमित कर दिया है। साथ ही किसी भी शहर के शोर रिकार्ड को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वाणिज्यिक, आवासीय, औद्योगिक और शांत।
यूएनईपी की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन का कहना है कि जैसे-जैसे शहर बढ़ रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसमें भी काफी तकनीकी पेंच हैं, जैसे- एसी व झींगुर की आवाज भले ही मानक स्तर के नीचे हो पर निरंतर होने से इरीटेशन होने लगता है और कान से लेकर दिमाग तक वही आवाज सनसनाती रहती है। खराब तरीके से बनाए गए अपार्टमेंट भी निवासियों को परेशान करते हैं। एसी, खराब पंखे, प्लंबिंग, बॉयलर, जेनरेटर का शोर और तोड़-फोड़ भी परेशानी का कारण बनते हैं।
बिना इंसुलेशन वाली दीवारें और छतें पड़ोसी इकाइयों से आने वाले संगीत, आवाजें, कदमों की आहट व अन्य गतिविधियों को प्रकट करती हैं। खिड़कियां खुली, खराब या चमकीली हों तो निवासियों को आपातकालीन वाहन, ट्रैफिक, कचरा संग्रहण और अन्य प्रकार के शोर सुनाई दे सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर और विभिन्न रसोई उपकरण भी बहुत से लोगों को इरीटेट करते हैं। शहरों के ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाजों की संख्या सड़कों पर चलने वाली कारों से कम जरूर है पर अधिकांश यात्री विमान 130 डीबी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। हालांकि यह गति, ऊंचाई और लड़ाकू विमानों के हिसाब से कम और अधिक हो सकती है।
छतों पर नाइट लाइफ, बार व रेस्तरां और कुत्ते के रोने या भौंकने की आवाज दिन में 60 तो रात में 80 डीबी तक हो सकती है। गौरतलब है कि शोर का उच्च स्तर टिनिटस या बहरापन पैदा कर सकता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। अत्यधिक तेज व लगातार शोर के कारण श्वसन संबंधी उत्तेजना, नाड़ी का तेज चलना, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस हो सकती है तो दिल की धड़कनें बहुत बढ़ने पर दौरा तक पड़ सकता है। शोर से मानव और पशु में परेशानी, थकान, अवसाद, चिंता, आक्रामकता और उन्माद हो सकता है। कुछ लोग अनिद्रा के भी शिकार हो सकते हैं। 45 डीबी से अधिक शोर नींद में खलल डालता है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने अब इसे घटाकर 30 डीबी की सिफारिश की है। शोर एकाग्रता में कमी तो लाता ही है और ध्यान व प्रदर्शन को भी खराब कर सकता है।
याददाश्त कमजोर होने से पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। विज्ञान कहता है कि 100 डीबीएस पर दो घंटे के शोर से उबरने के लिए कानों को 16 घंटे से ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है। शोध से पता चला है कि शहरी शोर पशु-पक्षियों के बीच संचार, शिकारियों का पता लगाने और प्रजनन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यह भी पता चला है कि तेज आवाज के कारण कैटरपिलर की पृष्ठीय वाहिकाएं तेजी से धड़कने लगती हैं तो ब्लू बर्ड को बच्चे कम होने लगे हैं। संगठन शोरगुल से भरी मौज-मस्ती वाली गतिविधियों से बचने, कारों की बजाय साइकिल या इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल और शोर सोखने वाली सामग्री से घरों को इंसुलेट करने की सलाह देता है।