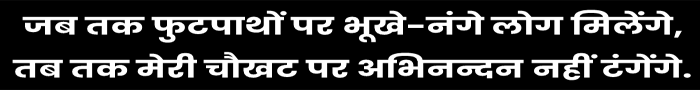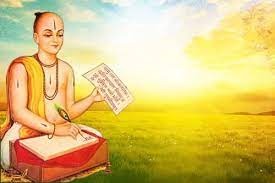
गोस्वामी तुलसीदास जी अथवा किसी भी महापुरुष के संसार में आगमन के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, वह है जीव का परम कल्याण। जीव का कल्याण शरीरक, मानसिक व आत्मिक स्तर पर होता है। ऐसा नहीं, कि संसार में अन्य समाज सेवी लोग यह प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन समस्या यह है, कि वे सफल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि धार्मिक ग्रंथों की यह दृढ़ मान्यता है, कि जगत में अगर सच में कोई सच में सेवा कर सकता है, तो वे संत-महापुरुष, स्वयं ईश्वर अथवा प्रभु के भक्त ही होते हैं।
एक साधारण जीव का हृदय इतना अपरिपक्व-सा होता है, कि उसपे आसानी से कोई भी रंग चढ़ जाता है। जिसके चलते संसार में मायावी जीवों की संख्या ज्यादा होती है। परिणाम स्वरूप ऐसे ही जीव पाप की ओर भी शीघ्रता से अग्रसर होते हैं। उन्हें लालच, वैमनस्य अथवा अन्य किसी भी अवगुण के प्रभाव में आने में अधिक समय नहीं लगता। समाज इन्हीं विकृत व पीड़ित सोच वाले लोगों से पीड़ित है। अब उन्हें कैसे सही मार्ग पर लाया जा सकता है? इसके लिए अनेकों सामाजिक संस्थायें अथक प्रयास भी कर रही हैं। लेकिन परिणाम आप सब के समक्ष दृष्टिगोचर है।
वहीं अगर यही दायत्व हमारे महापुरुष संभालते हैं, तो वे सर्वप्रथम एक ही कार्य करते हैं, वह यह कि वे उस जीव की संगति ही बदल देते हैं। संगति एक ऐसा माध्यम है, जिससे आप किसी भी मानव की वृति को आसानी से बदल सकते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं-
‘सठ सुधरहिं सतसंगति पाई।
पारस परस कुधात सुहाई।।
बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं।
फनि मनि सम निज बून अनुसतहीं।।’
अर्थात जैसे पारस के संग करने से कुधातु लोहा भी अमूल्य स्वर्ण बन जाता है, ठीक वैसे ही दुष्ट जन भी सतसंग के प्रभाव में आने से सुधर जाते हैं। उन्हें दैवीय गुणों की प्राप्ति होने लगती है। वे कौवे से हंस व बगुले से हंस की वृति धारण कर लेते हैं।
यहाँ मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि दुष्ट अगर संत का संग करने से बदल जाता है, उसपे संगति का प्रभाव होता है, तो संत पर दुष्ट की संगति का प्रभाव क्यों नहीं होता? इसका समाधान गोस्वामी जी बड़ी सुंदर उदाहरण से देते हैं। वे कहते हैं, कि मणि एक बहुत ही सुंदर व बहुमूल्य रतन है। उसका स्थान सर्प के सीस को माना गया है। सब जानते हैं, कि सर्प तो विशैला होता है, तो क्या उसके सीस पर सुशोभित मणि भी विषैली होती है? नहीं! सर्प का संग उस मणि को विशैला नहीं बना देता। ठीक इसी प्रकार से अगर संत जन किसी दुष्ट का संग कर लें, तो ऐसा नहीं कि उन पर उस दुष्ट का रंग चढ़ जायेगा।
अधिक क्या कहें, गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं, कि बिना सतसंग के जीव बुद्धिमान तो हो सकता है, लेकिन उसमें विवेक का समावेश नहीं हो सकता। प्रभु विवेक को ही प्राथमिकता देते हैं। कारण कि बुद्धि स्वार्थ सोचती है, और विवेक परमार्थ। विवेक ईश्वरीय विद्या है, और बुद्धि संसारिक विद्या से निर्मित है। विवेक किताबों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, और बुद्धि को अनुभव या किताबों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न उठता है, कि सतसंग में आखित ऐसा क्या होता है? सतसंग कुछ साधारण से प्रवचन ही तो होते हैं। यह प्रवचन हम किताबों में भी तो पढ़ सकते हैं। सज्जनों सतसंग का अर्थ केवल प्रवचन ही होता, तो ठीक है, कि हम वे किताबों में भी पढ़ लेते। लेकिन ऐसे एक से एक प्रवचन, क्या रावण ने ग्रंथों में से नहीं पढ़े होंगे? ऐसे में उसमें विवेक जाग्रित क्यों नहीं हुआ? कारण कि केवल अध्यन से विवेक नहीं आता। वह तो केवल सतसंग से ही आयेगा और सतसंग की परिभाषा कभी भी प्रवचन नहीं होती। भले ही संपूर्ण संसार में यही कहा जाता है, कि प्रवचन सुनना ही सतसंग है, लेकिन गोस्वामी जी श्रीरामचरित मानस में सतसंग की जो परिभाषा दे रहे हैं, उसे सुन आप दंग रह जायेंगे। उस सतसंग के प्रभाव के संबंध के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं-
‘मज्जन फल पेखिअ ततकाला।
काक होहिं पिक बकउ मराला।।
सुनि आचरज करै जनि कोई।
सतसंगति महिमा नहिं गोई।।’
अर्थात सतसंग का प्रभाव है ही ऐसा, कि अगर इसमें कोई कौवे जैसा क्रूर व्यक्ति भी हो, उसका भोजन भी निंदनीय हो। सबसे बड़ी बात कि उसकी बोली व भाषा भी अतिअंत निम्न स्तर की हो, लेकिन अगर वो एक क्षण के लिए भी सतसंग में आ जाये, तो वह कोयल की भाँति सुरीला अर्थात मृदु भाषी हो जाता है। साथ ही वह अभक्ष भोजन का त्याग कर सात्विक भोजन का सेवन करने लगता है।
दूसरा एक और उदाहरण देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, कि अगर किसी व्यक्ति की वृति बगुले जैसी भी हो। अर्थात वह व्यक्ति कपट व छल से भरा हुआ हो, लेकिन तब भी अगर उसे सतसंग प्राप्त हो जाये, तो वह हंस की भाँति सदाचारी हो जाता है। लेकिन प्रश्न तो यही है, कि अगर ऐसा सब कुछ इतनी सरलता से संभव है, तो इतने सतसंग होने के पश्चात भी जीव में परिवर्तन क्यों नहीं है? इसका कारण यही है, कि जिस सतसंग की चर्चा महापुरुष कर रहे हैं, वो सतसंग ही कुछ और है।